CTET CDP MARATHON आपके CTET प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है । आप CDP की तैयारी से पेपर 1 और पेपर 2 में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते है । Child Development and Pedagogy CTET एवं सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओ में पूछे जाते है | पर्यावरण अध्ययन CTET, UPTET, REET, MP TET और अन्य शिक्षण परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है |बाल विकास के नोट्स जो विभिन्न टीईटी परीक्षा के लिए तैयार हैं जो आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है | Child Development and Pedagogy in One-Shot आपके परीक्षा में लिए काफी महत्वपूर्ण है | बाल विकास के महत्वपुर्ण वन लाइनर प्रश्न उत्तर से आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं |
बाल विकास CTET, UPTET, REET, MP TET और अन्य शिक्षण परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है |Child Development and Pedagogy से बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रारूप में कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे की – CTET, UPTET, HPTET, PSTET,BPSC TET ,MPTET ,etc में पूछे जाते हैं | CTET CDP सिलेबस 2024 में इस खंड Environmental Studies से बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रारूप में कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इस पोस्ट में बाल विकास(CDP Pedagogy ) के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके उत्तर को देख पाएंगे | इसलिए Complete CTET CDP Marathon One Shot इस पोस्ट के माध्यम से पूरा जरुर देखें |
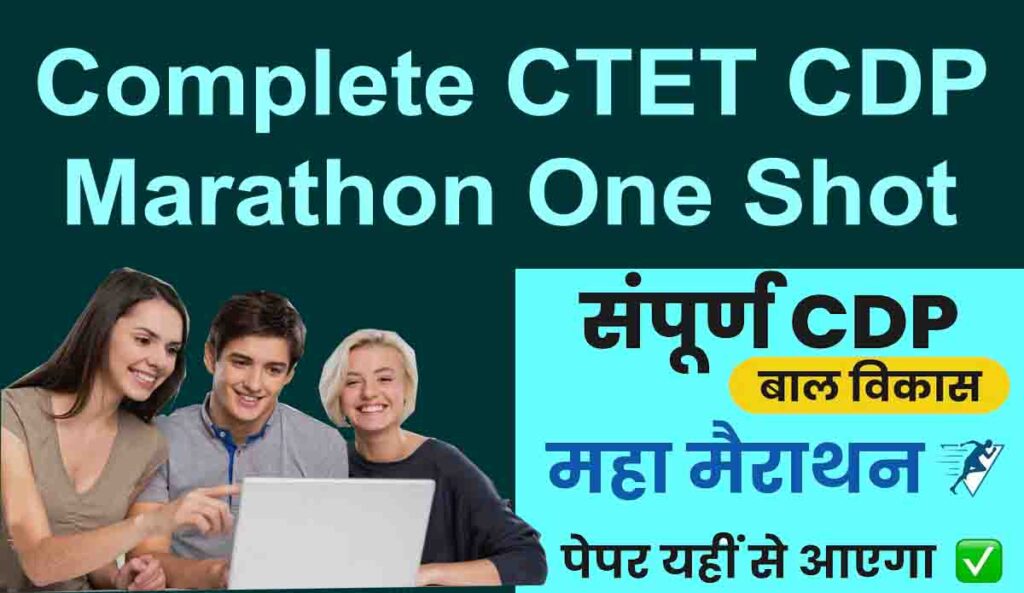
CDP Marathon Class for CTET
- विकास की कोई सीमा नही होती। विकास के सिद्धांत-विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हैं, क्योंकि बदलाव दिन-प्रतिदिन आते हैं। विकास जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलते रहता हैं
- विकास के निम्न सिद्धांत हैं-
- 1) विकास की दिशा का सिद्धांत (Principle of development direction
- 2) निरंतर विकास का सिद्धांत (Principle of continuous development)
- 3) व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत (Principle of individual differences)
- 4) विकास क्रम का सिद्धांत (Theory of evolution)
- 5) परस्पर संबंध का सिद्धांत (Reciprocal principle)
- 6) समान प्रतिमान का सिद्धांत (Principle of common pattern)
- 7) वंशानुक्रम सिद्धांत (Inheritance principle)
- 8) पर्यावरणीय सिद्धांत ( Environmental principles)
- विकास एकधारणीय और एका-आयामी होता है। जबकि विकास के बारे में यह सत्य है कि विकास ऊपर से नीचे की ओर तथा केन्द्र से बाहर की ओर होता है। विकास आनुवंशिकता और सम्पोषण से प्रभावित होता है।
- विकास सामाजिक-सांस्कृतिक परिपेक्ष में होता है। बाल विकास का सिद्धान्त है-
- (i) निरंतर विकास का सिद्धान्त
- (ii) विकास दिशा का सिद्धान्त
- (iii) वैयक्तिव विभिन्नता का सिद्धान्त
- (iv) क्रमबद्धता का सिद्धान्त
- (v) वंशानुगत व वातावरण की अंतर्क्रिया का सिद्धान्त ।
- शीर्षगामी सिद्धान्त विकास के ‘गामक विकास’ के क्षेत्र पर लागू होता है। विकास का शीर्षगामी सिद्धान्त में बालकों का विकास सिर से पैर तक होता है।
- बालक के शारीरिक विकास में मस्तिष्क और शरीर में वृद्धि और परिवर्तन शामिल है, जिनमें इंद्रिय अंग, गत्यात्मक कौशल, स्वास्थ्य आदि शामिल होता है।
- वह विकास जो शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है, उसे समीपोदूरस्थ विकास कहते हैं।
- बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, शुरूआत में सबसे पहले बालक सिर को उठाता है, फिर बैठना सीखता है, तश्पश्चात चलना सीखता है। इसे ही विकास की शीर्षगामी सिद्धान्त कहते हैं, जो गामक विकास के क्षेत्र पर लागू होता है।
- भाषा विकास के संदर्भ में ‘प्रारंभिक अवस्था’ बहुत ही संवेदनशील अवस्था होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा विकास में अति महत्त्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। इस अवस्था में आयु के साथ-साथ बालकों के सीखने की गति में वृद्धि होती है। प्रत्येक क्रिया के साथ भाषा विस्तार होती है। इस अवस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक की सभी क्रियाए सीख लेता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों को वस्तुओं को देखकर उसका प्रत्यय ज्ञान हो जाता है तथा अपने आस-पड़ोस तथा घर समुदाय में बच्चे सुनकर भाषा सीख लेता है।
- परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, प्रारंभिक समाजीकरण कहलाता है।
- बच्चा जब इस संसार में आता है तब वह कोरे कागज की तरह होता है, फिर धीरे-धीरे जैसे वह बड़ा होने लगता है अपने आस-पास के साधनों द्वारा प्रभावित होने लगता है तथा निरंतर वह आदर्शो व मूल्यों को सीखता है। इन आदर्शो व मूल्यों को वह अपने समाज (परिवार, साथी, स्कूल, शिक्षक) से सीखता है। इसे ही प्रारंभिक समाजीकरण कहते हैं।
- समाजीकरण के कुछ सक्रिय कारक है जैसे—परिवार, आस- पड़ोस, स्कूल, मित्रगण आदि।
- समाजीकरण के कुछ निष्क्रिय कारक भी होते हैं जैसे—पुस्तकालय, खेल का मैदान, आदि।
- लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धान्त के अनुसार ‘पारंपरिक चरण’ में नैतिक चिंतन शुरूआती सामाजिक परिपेक्ष पर आधारित होता है। पारंपरिक चरण या परंपरागत स्तर के बालक दूसरे के नैतिक मानको को अपने में आंतरीकृत करते हैं। उन मानको के सही/ गलत का निर्णय करते है तथा उस पर अपनी सहमति बनाते हैं तथा अपनी आवश्यकता के साथ-साथ दूसरे की आवश्यकता का भी ध्यान रखते हैं। इस स्तर के बालकों में नैतिक चिंतन शुरूआती समाजिक परिपेक्ष पर आधारित होता है। बालक समाज के नियम के अनुसार व्यवहार करने लगता है। तथा समाज से अनुमोदन पाना चाहते हैं। वे स्वयं को उत्तम लड़का, अच्छी लड़की कहलाना पसंद करते हैं।
- पियाजे के सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करना आत्मसात्करण कहते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बालक आत्मसात्करण और सामंजस्य की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। जब बच्चे के सामने कोई नई समस्या होती है, तो उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है। उस असंतुलन को दूर करने के लिए वह आत्मसात्करण या समंजन या दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभ करता है।
- ● जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धान्त में दो पदों का उपयोग किया—संगठन और अनुकूलन।
- अनुकूलन की सम्पूर्ण प्रक्रिया को दो उप प्रक्रियाओं में बांटा गया— आत्मसात्करण (Assimilation) समंजन (Accomoda- tion)
- स्वायत्त नैतिकता (Autonomous Morality) की अवस्था से इस काल में नैतिकता बच्चों के मित्रों के बीच के सम्बन्धों में विकसित होती है। अपने मित्रों के समकक्ष अर्थात मित्रास का एक ऐसा दर्शन उभरता है, जिससे दूसरे के अधिकारी को के दाम चिन्ता एवं पारस्परिकता का 11 वर्ष) भाव दिखता है। बच्चों में सोचने की प्रवृत्ति होती है नियम एवं कानून लोना द्वारा निर्मित किए गए हैं।
- लॉरेन्स कोह्लबर्ग का नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धान्त लॉरेन्स कोहवर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धान्त को आधार बनाकर नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धान्त दिया | कोहबर्ग का मानना है कि कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण दण्ड से स्वयं को बचाना है।
- सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने बालकों में सामाजिक विकास से सम्बन्धित एक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। इस सिद्धान्त में उन्होंने बताया कि बालक के हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है।
- आज की शिक्षा पद्धति बाल-केन्द्रित है। इसमें प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है पिछड़े (Backward) हुए और मन्दबुद्धि,बाल-केन्द्रित शिक्षा की विशेषताएँ बाल-केन्द्रित शिक्षा आधुनिक शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है।
- प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। बालकों की प्रवृत्ति, रुचियों एवं क्षमताओं के बारे में शिक्षक को जानकारी रखनी चाहिए।
- मूल्यांकन और परीक्षण शिक्षण से ही शिक्षक की समस्या हल नहीं हो जाती। उसे बालकों के ज्ञान और विकास का मूल्यांकन और परीक्षण (Evaluation and Test) करना होता है।
- सतत और व्यापक मूल्यांकन (CCE) का अर्थ छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से है, जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। यह एक बच्चे की विकास प्रक्रिया है, जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य एक ओर मूल्यांकन में निरन्तरता और व्यापक रूप से सीखने के मूल्यांकन पर तथा दूसरी ओर व्यवहार के परिणामों पर आधारित हैं।
- सर्वांगीण विकास का सिद्धान्त बालकों में उसके सभी पक्षों को (सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, खेल, नेतृत्व) विकसित करने पर बल देना चाहिए। इसके माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। 5. चयन का सिद्धान्त बालकों की योग्यता के अनुरूप ही विषय-वस्तु का चयन करना चाहिए। बालकों की मानसिक दशा का भी शिक्षण के दौरान ध्यान रखना चाहिए।
- बाल केन्द्रित शिक्षा के अन्तर्गत पाठ्यक्रम वातावरण के अनुसार, लचीला, ज्ञान पर केन्द्रित, रुचि पर आधारित, राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला, बालक के मानसिक स्तर के अनुरूप इत्यादि विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए।
- सुविधाहीन वर्गों से सम्बन्धित बच्चों के प्रवेश, उपस्थिति, प्रतिधारण एवं अध्ययन स्तरों में सुधार करके प्राथमिक शिक्षा के व्यापीकरण को बढ़ाने तथा प्राथमिक स्तर के छात्रों की पोषाहार स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से 15 अगस्त, 1995 को पोषाहार समर्थन के राष्ट्रीय कार्यक्रम मध्याह्न भोजन स्कीम की शुरुआत की गई।
- वर्ष 2002 में संविधान के 86 वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21ए के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था।
- इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त, 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया, जो 1 अप्रैल, 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का महत्त्व शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा-कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय है।
- अन्तर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते के अनुसार 18 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को बच्चा माना गया है, जिसे भारत सहित 142 देशों ने स्वीकृति प्रदान की है फिर भी 14-18 वर्ष आयु वर्ग की शिक्षा की बात इस अधिनियम में नहीं की गई है।
- बुद्धि (Intelligence) शब्द का प्रयोग सामान्यतः प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि के अर्थों में किया जाता है। यह वह शक्ति है, जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।
- मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, बुद्धि वह मानसिक शक्ति है, जो व्यक्ति के समस्त कार्यों का संचालन करती है तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है।
- वैश्लर के अनुसार, “बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिन्तन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है।” वुडवर्थ के अनुसार, “बुद्धि, कार्य करने की एक विधि है।
- बहुकारक सिद्धान्त इस सिद्धान्त के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। इस सिद्धान्त के अनुसार, बुद्धि कई तत्त्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्त्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। अतः सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती, बल्कि बुद्धि में कई स्वतन्त्र, विशिष्ट योग्यताएँ निहित रहती हैं, जो विभिन्न कार्यों को सम्पादित करती है। थॉर्नडाइक ने तीन प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया। ये बुद्धि हैं- अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि तथा यान्त्रिक बुद्धि।
- चिन्तन का एक मुख्य तत्त्व है। संकल्पनाएँ वस्तुओं, क्रियाओं, विचारों व जीवित प्राणियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। संकल्पना के अन्तर्गत किसी के लक्षण, जैसे-मीठा, खट्टा, किसी के भाव, जैसे-क्रोध, भय तथा दो या अधिक वस्तुओं के बीच सम्बन्ध जैसे-उससे अच्छा, इससे खराब आदि की बात की जाती है।