Hindi Grammar in Hindi : हिंदी व्याकरण हिंदी सीखने और बोलने के लिए आप ही महत्वपूर्ण होता है |हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने को हिन्दी व्याकरण(Hindi grammar) कहते है | हिन्दी भाषा सिखने और उच्चारण के लिए हिन्दी व्याकरण सीखना अनिवार्य होता है | जिस तरह से हम इंग्लिश बोलने में इंग्लिश ग्रामर का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार हिंदी व्याकरण का प्रयोग हम हिंदी सीखने और बोलने में करते हैं | यह BPSC Teacher Recruitment Exams ,UPTET , CTET , MPTET जैसे महत्वपूर्ण पतियोगिता परीक्षाओ के लिए महत्वपूर्ण है |
Hindi Vyakaran का अध्ययन यानि प्रेक्टिस कर लेना चाहिए, जिससे एक्साम के वक्त हमे कोई डॉउट ना रहे |आज हम इस पोस्ट के माध्यम से हिंदी व्याकरण के संपूर्ण भाग को देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि Sampurn Hindi Vyakaran में कौन-कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है और आपके आने वाले एग्जाम में कहां-कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं | इसका अध्ययन यानि प्रेक्टिस कर लेना चाहिए, जिससे एक्साम के वक्त हमे कोई डॉउट ना रहे | यह आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद रूप साबित होंगे| हिंदी व्याकरण से आपको हिंदी बोलने की शुद्धता एवं हिंदी में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण वर्णों का ज्ञान होता है |
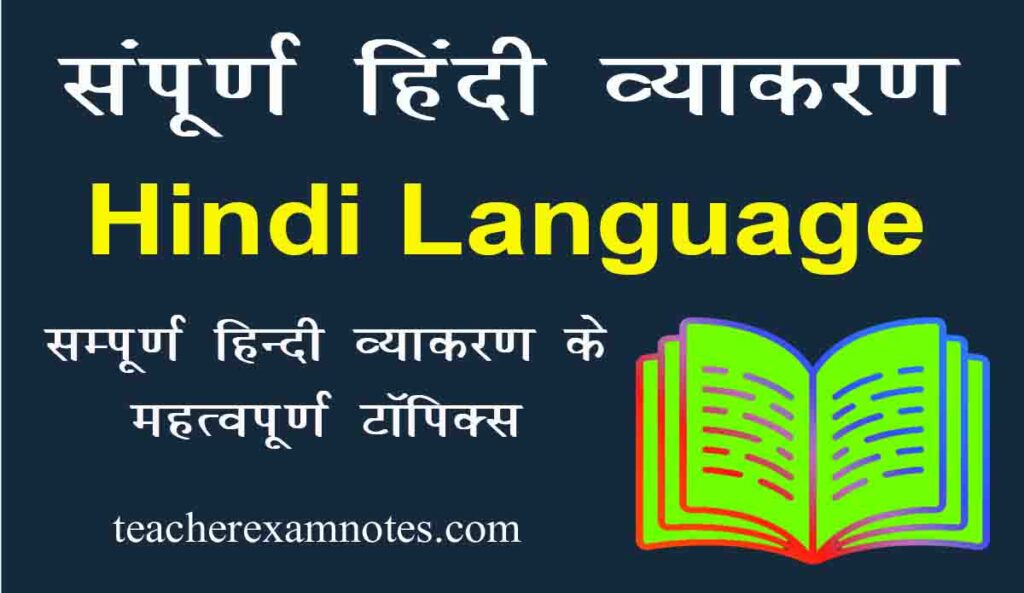
हिन्दी व्याकरण | Sampurna Hindi vyakaran | Hindi vyakaran Chart
हिन्दी व्याकरण किसे कहते है ?
हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने को हिन्दी व्याकरण कहते है | हिन्दी भाषा सिखने और उच्चारण के लिए हिन्दी व्याकरण सीखना अनिवार्य होता है |
हिन्दी भाषा को धाराप्रवाह बोलना, पढ़ना और लिखना हिन्दी व्याकरण के माध्यम से संभव है | हिंदी व्याकरण में वर्ण ,शब्द, भाषा, वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, पर्यायवाची, मुहावरे, रस, छंद, अलंकार इत्यादि सीखते है |
हिंदी भाषा का इतिहास लगभग एक हजार वर्ष पुराना माना गया है। संस्कृत सभी भाषाओ की जननी है | संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है और हिंदी का जन्म संस्कृत से ही हुआ है |
संस्कृत के बाद पालि भाषा का विकास हुआ |पालि के बाद प्राकृत भाषा का विकास हुआ | प्राकृत भाषा पहली ईस्वी से लेकर 500 ई. तक रही।
प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश का विकास हुआ यह 500 ई. से 1000 ई. तक माना गया है और अपभ्रंश के ही जो सरल और देशी भाषा शब्द थे उसे अवहट्ट कहा गया और अवहट्ट से ही हिंदी का उद्भव हुआ है ।
अवहट्ट नाम का जिक्र मैथिल महान कवि कोकिल विद्यापति की ‘कीर्तिलता’ में आता है।
महाकवि विद्यापति कई भाषाओं के ज्ञाता थे।इनकी अधिकांश रचना संस्कृत एवं अवहट्ट में है।
हिंदी भाषा का विकास के क्रम
संस्कृत → पालि → प्राकृत → अपभ्रंश → अवहट्ट → हिंदी
भारत में हिंदी का तेजी से विकास स्वन्त्रता आदोलन और हिंदी पत्रकारिता के कारण हुई है। भारत के स्वतन्त्र होने के बाद 14 सितंबर 1949 को हिन्दी को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया।
हिंदी आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी द्वारा बोली और समझे जानी वाली भाषा है। हिन्दी को आज 18% लोग पूरी दुनिया में बोलते है | हिंदी को हम भाषा की जननी, साहित्य की गरिमा, जन-जन की भाषा और राष्ट्रभाषा भी कहते हैं।
हिन्दी विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राजभाषा है।
हिंदी भाषा का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 17 एवं 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 351 में है।
8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषा
8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं की संख्या 22 है।
भारतीय भाषाओं की संख्या 22 है – कश्मीरी, सिन्धी, पंजाबी, हिन्दी, बंगाली, आसामी, उडिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मढिपूडी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली।
वैसे राज्य जहाँ अधिक हिन्दी बोली जाती है :-बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
यह भी पढिये :-
हिन्दी वर्ण, वर्णमाला, परिभाषा, भेद और उदाहरण
ध्वनियों को व्यक्त में जो लिपि-चिह्न का प्रयोग होता है उसे ‘वर्ण’ कहते हैं। वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई हैं। वर्ण के खंड या टुकड़े नहीं किये जा सकते है | हिन्दी में इन वर्णों को ‘अक्षर’ भी कहा जाता है। जैसे- अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, क, ख आदि।
वर्णमाला– वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं।
हिन्दी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। पहले स्वर वर्णों तथा बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है।
- मूल वर्ण – 44 (11 स्वर, 33 व्यंजन) – “अं, अः, ड़, ढ़, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र” को छोड़कर
- उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण – 47 (10 स्वर, 37 व्यंजन) – “ऋ, अं, अः, ड़, ढ़” को छोड़कर
- कुल वर्ण – 52 (13 स्वर, 39 व्यंजन)
- लेखन के आधार पर वर्ण – 52 (13 स्वर, 39 व्यंजन)
- मानक वर्ण – 52 (13 स्वर, 39 व्यंजन)
हिंदी में स्वर
जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र हो और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायता करते हो उसे स्वर कहते है।
स्वर संख्या में कुल 13 हैं- अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ अं, अः।
हिंदी में स्वर तिन प्रकार के होते है _
- ह्रस्व स्वर
- दीर्घ स्वर
- प्लुत स्वर
व्यंजन
जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं।
व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते है ।
व्यंजन संख्या में कुल 39 हैं।
व्यंजन के तीन भेद
- स्पर्श
- अंतःस्थ
- ऊष्म
अनुस्वार और अनुनासिक
अनुस्वार (Anushwar) :- अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका चिन्ह (ं) है। ङ्, ञ़्, ण्, न्, म् – ये पंचमाक्षर कहलाते हैं|
जैसे- सम्भव=संभव, सञ्जय=संजय, गड़्गा=गंगा।
अनुनासिक (Anunasik – चंद्रबिंदु) :- जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से हो तब उसके ऊपर चंद्रबिंदु (ँ) लगता है।
जैसे-हँसना, आँख।
विसर्ग और हलंत क्या होते है ?
विसर्ग :- ब्राह्मी से उत्पन्न विसर्ग ( ः ) महाप्राण सूचक एक स्वर है।
रामः, प्रातः, अतः, सम्भवतः, आदि में अन्त में विसर्ग आया है।
हलंत:- व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा (्) लगा दी जाती है।
जैसे-विद्यां।
काल (Tense)
काल :- समय अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का ज्ञान हो उसे ‘काल‘ कहते हैं।
काल (Tense) तीन प्रकार के होते हैं-
- वर्तमान काल
- भूतकाल
- भविष्यत् काल
वर्तमान काल :- क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का ज्ञान हो उसे वर्तमान काल कहते हैं।
वाक्यों के अंत में है, हैं, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं।
जैसे- मैं आम खता हु|
वर्तमान काल के छः (6) भेद होते हैं-
- सामान्य वर्तमान काल
- अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल
- पूर्ण वर्तमान काल
- संदिग्ध वर्तमान काल
- संभाव्य वर्तमान काल
- पूर्ण सातत्य वर्तमान काल
भूतकाल :- जो समय बीत चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं|
जैसे- वर्षा हुई थी।
भूतकाल के छह (6) भेद हैं-
- सामान्य
- आसन्न
- पूर्ण
- अपूर्ण
- संदिग्ध
- हेतु-हेतुमद् भूतकाल
भविष्यत् काल :-क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय के बोध हो, उसे भविष्यत् काल कहते हैं|
जैसे- राम खेलेगा।
भविष्यत् काल के चार (4) भेद हैं-
- सामान्य
- सम्भाव्य
- सातत्यबोधक
- हेतु-हेतुमद् भविष्यत् काल
विराम चिन्ह क्या होते है ?
विराम चिन्ह का मतलब है ठहराव, विश्राम, रुकना।
विराम चिह्न के प्रकार:
- अल्प विराम (Comma)( , )
- अर्द्ध विराम (Semi colon) ( ; )
- पूर्ण विराम (Full-Stop) ( । )
- योजक चिह्न (Hyphen) ( – )
- अवतरण चिह्न या उद्धरण चिह्न (Inverted Comma) ( ”… ” )
- लाघव चिह्न (Abbreviation sign) ( o )
- आदेश चिह्न (Sign of following – विवरण चिन्ह) ( :- )
- रेखांकन चिह्न (Underline) ( _ )
- लोप चिह्न (Mark of Omission – पदलोप चिन्ह)( … )
- पुनरुक्ति सूचक चिन्ह-Repeat Pointer Symbol (,,)
- विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह-Oblivion Sign ( ^ )
- दीर्घ उच्चारण चिन्ह ( S )
- तुल्यता सूचक चिन्ह ( = )
- निर्देशक चिन्ह ( ― )
- उप विराम (Colon) [ : ]
- विस्मयादिबोधक चिह्न (Sign of Interjection)( ! )
- प्रश्नवाचक चिह्न (Question mark) ( ? )
- कोष्ठक (Bracket) ( ( ) )
संज्ञा और संज्ञा के रूप
संज्ञा :- वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध होता हैं।
जैसे- श्याम, आम, मिठास, हाथी आदि।
संज्ञा के प्रकार:-
- जातिवाचक
- व्यक्तिवाचक
- भाववाचक संज्ञा
पद वह है जिसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह व्याकरण के नियमों में बँध जाता है और इसका रूप भी बदल जाता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द न कहकर पद कहा जाता है।
हिन्दी में पद पाँच प्रकार के होते हैं-
- संज्ञा
- सर्वनाम
- विशेषण
- क्रिया
- अव्यय
लिंग (GENDER)
जो शब्द स्त्री व पुरुष में भेद उत्त्पन्न करता है, उसे लिंग कहते है। या वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, आदि में स्त्री-पुरुष होने का ज्ञान कराता हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं: 1. पुल्लिंग 2. स्त्रीलिंग।
वचन (NUMBER)
जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं।
हिंदी में मुख्य रूप से एकवचन और बहुवचन होते है।
कारक (CASE)
वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे पूरी घटना या उद्देश्य की पूर्ति हो, उसे कारक कहते हैं।
कारक चिन्ह प्रयोग/विभक्ति/परसर्ग:
- कर्ता कारक (NOMINATIVE CASE) – ने [ राम ने रावण को मारा , लड़की स्कूल जाती है। ]
- कर्म कारक (OBJECTIVE CASE) – को [ लड़की ने सांप को मारा , मोहन ने पत्र लिखा। ]
- करण कारक (INSTRUMENTEL CASE) – से , के , साथ , [ अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा , बालक गेंद से खेल रहे हैं। ]
- संप्रदान कारक (DATIVE CASE) – के लिए , [ गुरुजी को फल दो। ]
- अपादान कारक (ABLATIVE CASE) – से , [ बच्चा छत से गिर पड़ा , संगीता घोड़े से गिर पड़ी। ]
- संबंध कारक (RELATIVE CASE) – का , के , की [ वह मोहन का बेटा है , यह कमला की गाय है। ]
- अधिकरण कारक (LOCATIVE CASE) – में , पर [ भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। ]
- संबोधन कारक (VOCATIVE CASE) – हे ! हरे ! [ अरे भैया कहां जा रहे हो , हे राम ! ( संबोधन )]
सर्वनाम क्या होते है ?
सर्वनाम वह होता है जो प्रश्नाधीन व्यक्ति के नाम की जगह पर मौजूद है।
हिंदी के मूल सर्वनाम 11 हैं- मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ।.
प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 हैं-
- पुरुषवाचक सर्वनाम
- निश्चयवाचक सर्वनाम
- अनिश्चयवाचक सर्वनाम
- संबंधवाचक सर्वनाम
- प्रश्नवाचक सर्वनाम
- निजवाचक सर्वनाम
यह भी पढिये :-
विशेषण क्या होते है ?
संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता (गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि) बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं।
जैसे – बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुन्दर, कायर, टेढ़ा-मेढ़ा, एक, दो आदि।
विशेषण के 4 प्रकार हैं-
- गुणवाचक विशेषण
- संख्यावाचक विशेषण
- परिमाणवाचक विशेषण
- सार्वनामिक विशेषण
क्रिया क्या होते है ?
जिस शब्द अथवा शब्द-समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किये जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं।
जैसे- सीता ‘नाच रही है’।
क्रियाविशेषण क्या होते है ?
जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रियाविशेषण कहते हैं।
जैसे – वह धीरे-धीरे चलता है।
क्रियाविशेषण के चार प्रकार है :
- स्थानवाचक
- कालवाचक
- परिमाणवाचक
- रीतिवाचक
उपसर्ग क्या होते है ?
जो शब्दों के शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं।
हिंदी व्याकरण में प्रमुख उपसर्ग की संख्या 13 है, जबकि संस्कृत में प्रमुख उपसर्गों की संख्या 22 है।
जैसे :- अ + छूता- अछूता
हिन्दी में उपसर्ग के मुख्यतः तीन प्रकार के भेद होते हैं-
- तत्सम उपसर्ग
- तद्भव उपसर्ग
- आगत उपसर्ग
समास क्या होता है ?
समास का मतलब है ‘संक्षिप्तीकरण’।
हिन्दी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप
जैसे :- रसोई के लिए घर = रसोईघर
समास के भेद (Samas ke bhed)
- अव्ययीभाव समास
- तत्पुरुष समास
- कर्मधारय समास
- द्विगु समास
- द्वन्द समास
- बहुव्रीहि समास
अलंकार क्या होते है ?
अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है- ‘आभूषण’,
जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहते है।
अलंकार को व्याकरण शास्त्रियों ने उनके गुणों के आधार पर तीन भी किया हैं – शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार।
विलोम शब्द‘ या ‘विपरीतार्थक शब्द किसे कहते है ?
जिस शब्द से अपने निश्चित अर्थ होते हैं,और उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द ‘विलोम शब्द‘ या विपरीतार्थक शब्द (Antonyms) कहलाते हैं।
जैसे: भाई-बहन
तत्सम शब्द या तद्भव शब्द
तत्सम शब्द: तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों, तत् + सम् से मिलकर बना है।
तत् का अर्थ है –उसके, तथा सम् का अर्थ है – समान।
तद्भव शब्द: तद्भव शब्द दो शब्दों तत् + भव से मिलकर बना है।
जिसका अर्थ है – उससे उत्पन्न। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं |
पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द क्या है |
जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते है।
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द
हिंदी अनेक शब्द के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं।
हिंदी भाषा में कई शब्दों की जगह पर एक शब्द बोलकर भाषा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है।
एकार्थक शब्द
बहुत से शब्द ऐसे हैँ जिनका अर्थ देखने और सुनने में एक सा लगता है, परन्तु वे समानार्थी नहीं होते हैं। .
अनेकार्थक शब्द
अनेकार्थक शब्द किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ होना। बहुत से शब्द ऐसे हैं, जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं।
Muhavare (Idioms) (मुहावरे) और लोकोक्तियां
मुहावरा: सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विशेष अथवा विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले पदबन्ध को मुहावरा कहते हैँ।
लोकोक्ति :- हिन्दी भाषा में बहुत अधिक प्रचलित और लोगों के मुँहचढ़े वाक्य लोकोक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। इन वाक्यों में जनता के अनुभव का निचोड़ या सार होता है। देखे –लोकोक्तियाँ
हिन्दी के प्रमुख कवि या लेखक और रचनाएँ – पद्य लेखक
पद्य (काव्य, कविता), साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है।
आपको यह संपूर्ण हिंदी व्याकरण की जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं और अगर यह आप लोगों को अच्छी लगती हो तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें जिससे हमें प्रोत्साहन मिले |